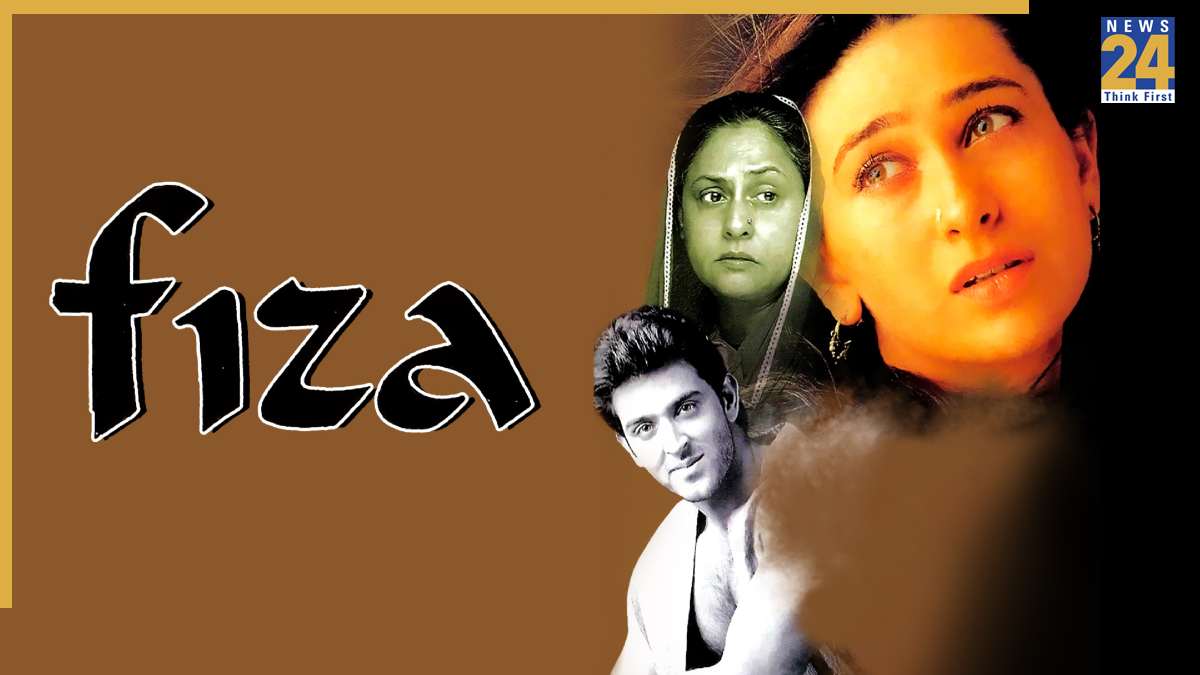अपनी रिलीज़ के 25 साल बाद, फ़िल्मकार ख़ालिद मोहम्मद फ़िज़ा के निर्माण, विषयों और चिरस्थायी प्रभाव को याद करते हैं। एक स्टार-स्टडेड कास्ट को निर्देशित करने से लेकर संवेदनशील सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने तक, मोहम्मद इस कहानी को पर्दे पर लाने के दौरान अपने अनुभवों, प्रेरणाओं और चुनौतियों को साझा करते हैं। इस स्पष्ट बातचीत में, वह फ़िज़ा की यात्रा पर फिर से जाते हैं, जो दशकों बाद भी प्रासंगिक बनी हुई है।
ख़ालिद, फ़िज़ा – आपके फ़िल्मकार के तौर पर सबसे बेहतरीन काम को 25 साल हो गए हैं, आप उस अनुभव को कैसे देखते हैं?
अशिष्ट लगने के खतरे में पड़कर, हाँ, मेरा मानना है कि सिनेमाई और विषय-वस्तु दोनों से, 1992-93 के दंगों के बाद के परिणामों के विरुद्ध, मुझे लगता है कि मैं फ़िज़ा के साथ निर्देशन करने में शामिल होने के बिना अधूरा और बेकार होता। ए. आर. रहमान द्वारा रचित और फ़िल्माया गया ‘क़व्वाली पिया हाजी अली’, धर्मनिरपेक्षता के एक ज़रूरी तत्व को दर्शाने के तौर पर बनाया गया था, जिसका असर हुआ, और इसी तरह यह संदेश भी दिया गया कि समुदायों के ध्रुवीकरण के पीछे अलग-अलग निहित राजनीतिक हित हैं, चाहे वह किसी भी आस्था से हो।
आपके फ़िल्मकार के तौर पर प्रेरणास्रोत कौन थे?
निर्देशक कोस्टा-गावरास (Z और स्टेट ऑफ़ सीज) के काम से प्रेरित होकर, मैंने उनकी गति और संपादन की शैली को बरकरार रखा, जिसमें श्रीकर प्रसाद के संपादन, संतोष सिवन की सिनेमैटोग्राफी और रंजीत बारोट के बैकग्राउंड संगीत ने बहुत मदद की, जिनका योगदान फ़िल्म की शुरुआत में माँ (मेरे दिवंगत दादा) को समर्पित है, जो बहुत संवेदनशील है। कुल मिलाकर अनुभव एक सहज रहा, बेशक कई बाधाएँ थीं, लेकिन मैं शांत रहा। फ़िज़ा होना ही था।
समीक्षाएँ बहुत प्रतिकूल थीं, है ना?
आज तक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पत्रकारिता बिरादरी इतनी प्रतिकूल क्यों थी, जिसने मुझे उन समीक्षाओं से भर दिया जो व्यक्तिगत रूप से मुझे निशाना बना रही थीं, फ़िल्म को नहीं। प्रतिष्ठित ट्रेड मैगज़ीन ने इसे फ्लॉप घोषित कर दिया, जबकि अगर आप बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन को गूगल करते हैं, तो यह 7 करोड़ रुपये के बजट पर बनी थी और 32 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए। ऐसा हो सकता है, श्याम बेनेगल सर के लिए लिखी गई मम्मो और ज़ुबैदा की स्क्रिप्ट, और फ़िज़ा, वे ऐसी हैं जिनसे आज तक मेरी पहचान है। एक तरफ़, मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने पेरिस की एक यात्रा के दौरान कोस्टा-गावरास से बात की, जहाँ वह रुके थे, उनसे पूछा कि क्या ऐसी फ़िल्म बनाना कोई मुद्दा है जो आतंकवाद विरोधी अपील करता है और उन्होंने जवाब दिया, “कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। विषय पर हर फ़िल्म मायने रखती है, कृपया कोई आत्म-संदेह न करें।”
आपके पास फ़िल्म में एक ज़बरदस्त कास्ट थी: जया बच्चन, ऋतिक रोशन, मनोज बाजपेयी, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन…हे भगवान, क्या यह मनमोहन देसाई की मल्टीस्टारर थी, या क्या!
मनमोहन देसाई के साथ तुलना एक मज़ाक है। मेरे कलाकारों में से कोई भी उस समय बड़े स्टार नहीं थे। मिस्टर बच्चन और शाहरुख खान को कैमियो करना था, लेकिन मुझे लगा कि यह दिखावटी और एक अनावश्यक व्यावसायिक घटक होगा, इसलिए मैंने उनकी उपस्थिति को स्क्रिप्ट से हटा दिया। जयाजी, एक सख्त टास्कमास्टर, ने स्क्रिप्ट पढ़ी और हामी भरी। ऋतिक रोशन जो कहो ना…प्यार है! पूरा कर रहे थे, मुझे याद है कि मैंने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई और एक घंटे बाद उन्होंने कहा “हाँ,” मैं भगवान दादा में एक बाल कलाकार के रूप में उनके प्रदर्शन से अभिभूत हो गया था, लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि उनकी आँखें इतनी भावुक हैं कि वह अमान के तौर पर अपनी पीड़ा को व्यक्त करने से आगे जा सकते हैं, जो संवादों में लिखे गए हैं। अमान के रूप में उनके प्रदर्शन का आज शायद ही कभी ज़िक्र होता है, लेकिन मेरे लिए, यह हमेशा अमूल्य रहेगा। करिश्मा कपूर को ज़ुबैदा और फ़िज़ा की स्क्रिप्ट एक ही समय पर ऑफ़र की गई थीं। उस वक़्त उन्हें ऐश्वर्या राय की भूमिका के लिए मोहब्बतें के लिए भी संपर्क किया गया था, लेकिन एक बार फिर मुझे लक मिला। उन्होंने दोनों फ़िल्में की, और उन्हें सबसे मुश्किल सीन—ख़ासकर उनकी दबी हुई चीख़ और एक अख़बार के संपादक के साथ एक सीन, जिसे वह कोसती हैं—में अभिनय करते देखना न केवल मेरा, बल्कि पूरी यूनिट का भी जबड़ा गिरा गया। मनोज बाजपेयी और सुष्मिता सेन, दोनों तुरंत सहमत हो गए। सुष्मिता ने मस्त माहौल… की शुरुआती रिकॉर्डिंग सुनी थी और उदयपुर में कम से कम छह से सात अलग-अलग जगहों पर तीन दिनों में यह नंबर शूट किया था, बीच-बीच में अपनी कार में झपकी लेते हुए। वैसे भी, यह एक औपचारिक स्टार प्रोजेक्ट नहीं था… जब हमने शुरुआत की तो करिश्मा सबसे बड़ी स्टार थीं। और ऋतिक, फ़िज़ा की शूटिंग के बीच में कहो ना प्यार है से रातोंरात सनसनी बन गए। वह स्टारडम से अप्रभावित रहे, और बम्बई के दूर-दराज़ के स्थानों पर शूटिंग तक पहुँचने के लिए मॉनसून की बाढ़ से भी गुज़रते थे।
क्या ये सभी आपकी पहली पसंद थे? मुझे याद है कि मेरे जानने वाले हर कोई जो मायने रखता था, फ़िज़ा का हिस्सा बनना चाहता था…क्या किसी ने सच में आपको मना किया?
नादिरा ज़हीर बब्बर ने विनम्रता से वह रोल निभाने से इनकार कर दिया जो आख़िरकार आशा सचदेव ने शानदार ढंग से निभाया। और एक अजीब वाक़या हुआ: मेरे सह-निर्माता प्रदीप गुहा ने कहा कि अक्षय कुमार दिलचस्पी रखते थे, हालाँकि मैं नहीं चाहता था। मैंने उन्हें वह रोल निभाने के लिए स्क्रिप्ट सुनाई जो बाद में विक्रम सालुजा ने निभाया। अक्षय अमान, फ़िज़ा के भाई बनना चाहते थे। मैं जितनी जल्दी हो सका उनके दफ़्तर से भागा। यह गलत कास्टिंग का मामला होता।
उस विशाल कास्ट को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था? आपने गुस्सा आने और अहंकार की टक्कर को कैसे संभाला?
कलाकार सहयोगी थे। यह निर्देशन में मेरा पहला मौक़ा था, और मुझे याद है कि जयाजी ने एक बार मुझसे पूछा था, “आप इतने शांत कैसे रहते हैं?” यह व्यावहारिक नहीं लगता, लेकिन मैं शांत था क्योंकि मुझे पता था कि कोई ऊपर मुझे पसंद करता है, मेरी दादी, जिसकी याद मेरे चारों ओर घूमती रही। उनके आख़िरी शब्द मेरे लिए थे, “कभी किसी के मोहताज मत बनना।” बेशक, मैं पूरी टीम पर निर्भर था जो उच्च क्षमता की थी। और हाँ, मुझे कुछ दृश्यों के लिए 100 से ज़्यादा लोगों की टीम को लीड करना अजीब लगा, क्योंकि मैं कोई रिंगमास्टर नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो फ़िल्म निर्देशित करना सांस लेने जितना ही सहज हो सकता है। उदयपुर में मस्त माहौल की शूटिंग के दौरान, जिसमें ऋतिक के सीन शामिल थे, मैं केवल उस वक़्त उलझन में था। वह राष्ट्र का क्रेज़ बन गए थे और कलेक्टर से लेकर शीर्ष पुलिस अफ़सरों तक, हर कोई उनके लिए पार्टियाँ देना चाहता था। संभव नहीं था। इसलिए गाने को गुरिल्ला स्टाइल में शूट किया गया, हम एक विशाल कुएँ वाले खेत और ईंटों के भट्टों में घुस गए। और जब ऋतिक को एक्शन सीन करना पड़ता था, तो मैं अपनी आँखें बंद कर लेता था, उनमें इतनी यथार्थवादी तरीके से काम करने की प्रतिभा थी कि उन्हें चोट लग जाती थी, जैसे एक बार उनके हाथ में चाकू लगने से खून बह गया, लेकिन वह विचलित नहीं हुए, कुछ एंटीसेप्टिक लगाया और बिना आधा शिकन किए जारी रखा।
फ़िज़ा ने एक ऐसे मुद्दे से निपटा जो आज भी पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है: मुस्लिम पहचान। आज आप फ़िज़ा के बारे में कितना गहरा महसूस करते हैं?
मैं गहरा महसूस नहीं करता। मैं अलगाव और गैर-समावेशिता के उदय से फट गया हूँ। मैंने केवल मुस्लिम किरदारों और उनकी परिस्थितियों, उनके आसपास की ‘फ़िज़ा’ के साथ ही फ़िल्में निर्देशित और लिखी हैं। आज कोई फाइनेंसर/निर्माता उन्हें नहीं चाहता। तो कम से कम पर्दे पर, मेरी कहानियों का अंत।
यह आज भी व्यापक रूप से माना जाता है कि पत्रकार अयोग्य फ़िल्मकार होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने उन्हें ग़लत साबित किया?
आप पत्रकारिता के पुराने स्कूल की बात कर रहे हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं था या किसी को सही या ग़लत साबित करने का इरादा नहीं था। अगर उनमें से ज़्यादातर, ख़ासकर स्टारडस्ट और इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे ने फ़िल्म की आलोचना की, तो ठीक है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली समीक्षा विदुषी मैथिली राव की थी जिन्होंने ब्रिटेन की बेहतरीन पत्रिका, साइट एंड साउंड में लिखा था, इस बात से हैरान थीं कि कैसे मणि कौल की फ़िल्में पसंद करने वाला कोई व्यक्ति यू-टर्न ले सकता है। वह भूल गई कि मैं मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा दोनों का प्रशंसक रहा हूँ। शायद मुझे उन्हें संजय लीला भंसाली की ख़ामोशी: द म्यूज़िकल, आदित्य चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और करण जौहर की कुछ कुछ होता है कि मेरी समीक्षाएँ भेजनी चाहिए थीं। लेकिन रहने दो, हर एक का अपना है।
अंत में, आप फ़िल्म जगत से इतने अलग क्यों हैं?
मैं अलग हो गया हूँ क्योंकि मुझे श्रद्धांजलि, पुरानी यादों के टुकड़े और राष्ट्र की अनजाने में या जानबूझकर प्रचार फ़िल्मों को लिखने के लिए कमीशन किया जा रहा था। स्वर्ग के लिए, तथ्य यह है कि एक बार जब आप खुद कुर्सी पर नहीं होते हैं, तो आपको उनकी ज़रूरत उनसे ज़्यादा होती है। तो नहीं, धन्यवाद। सुभाष, मैं दूसरे गोलार्ध में हूँ। मैंने तीन किताबें लिखी हैं, एक थिएटर प्ले का निर्देशन किया है और तीन वृत्तचित्र बनाए हैं, जिनमें श्याम बेनेगल को 90 मिनट की श्रद्धांजलि भी शामिल है। साथ ही मैंने दो और उपन्यास पूरे किए हैं (एक का अस्थायी शीर्षक द इम्परफेक्ट प्रिंस है और दूसरा बॉलीवुड के अंदर होने पर एक संस्मरण है)। मैं कभी-कभार पेंटिंग करता हूँ। मेरे लिए इतना काम बहुत है।